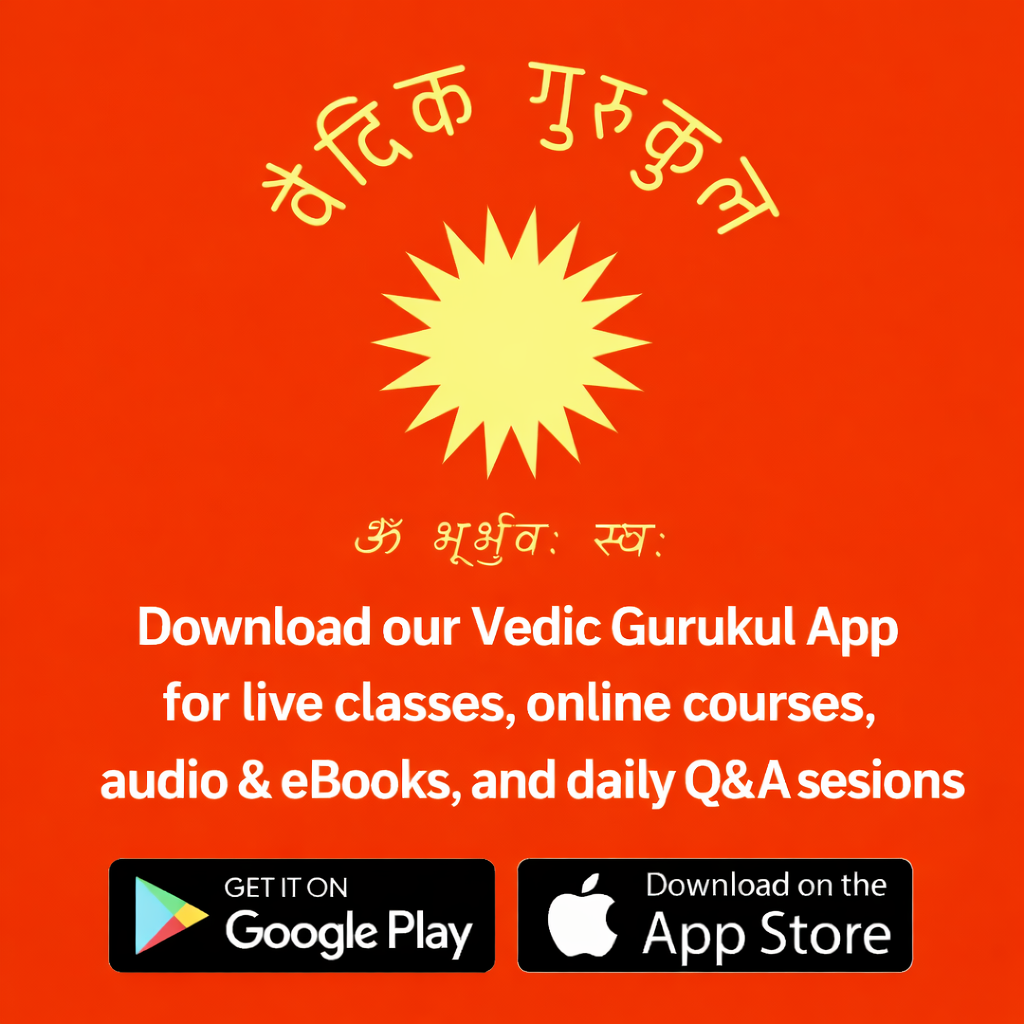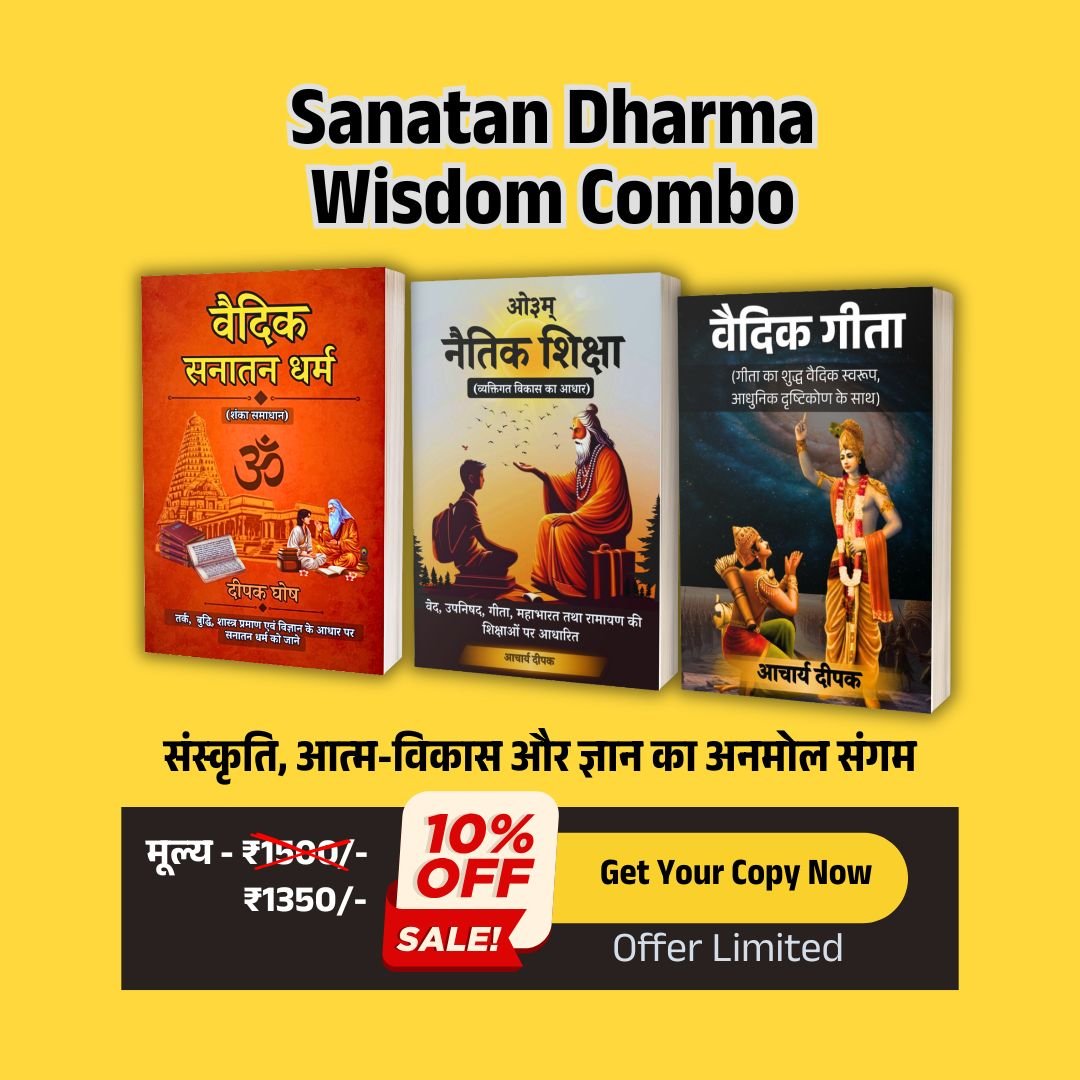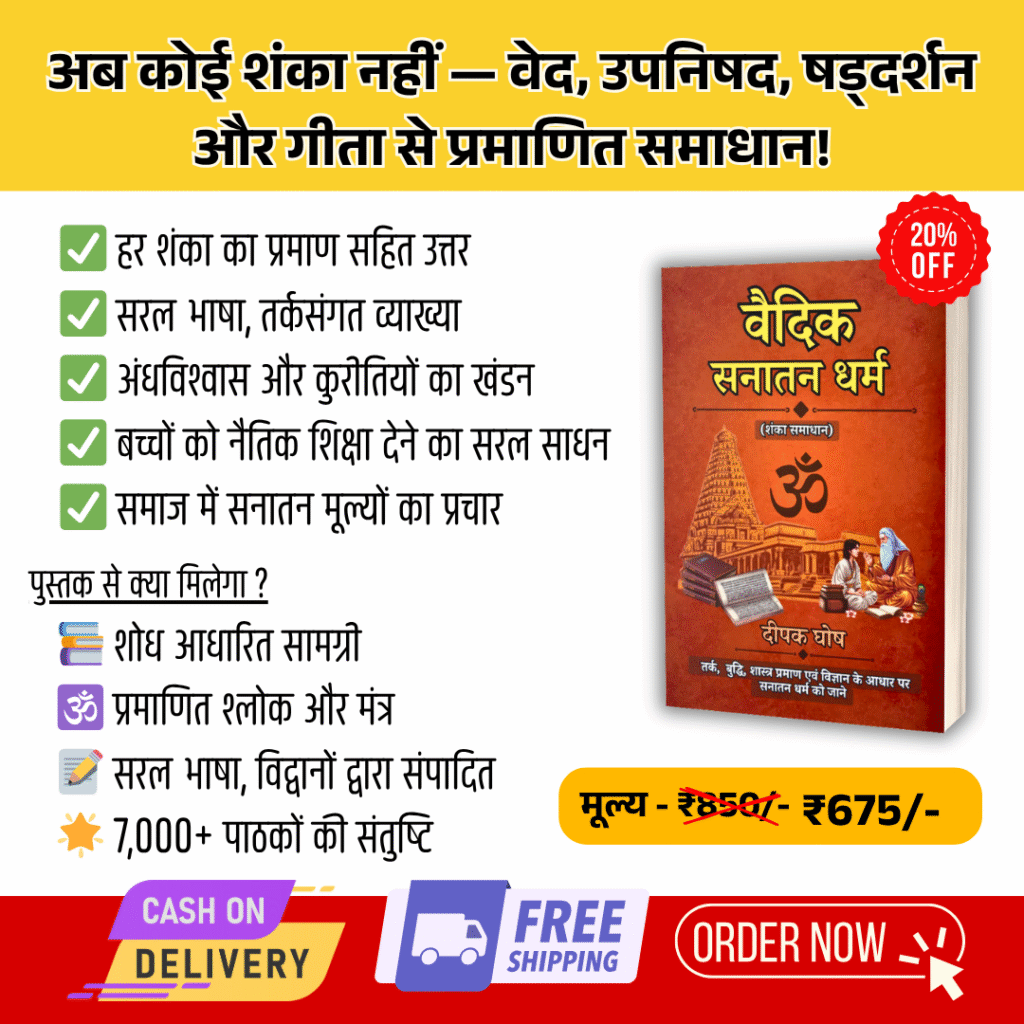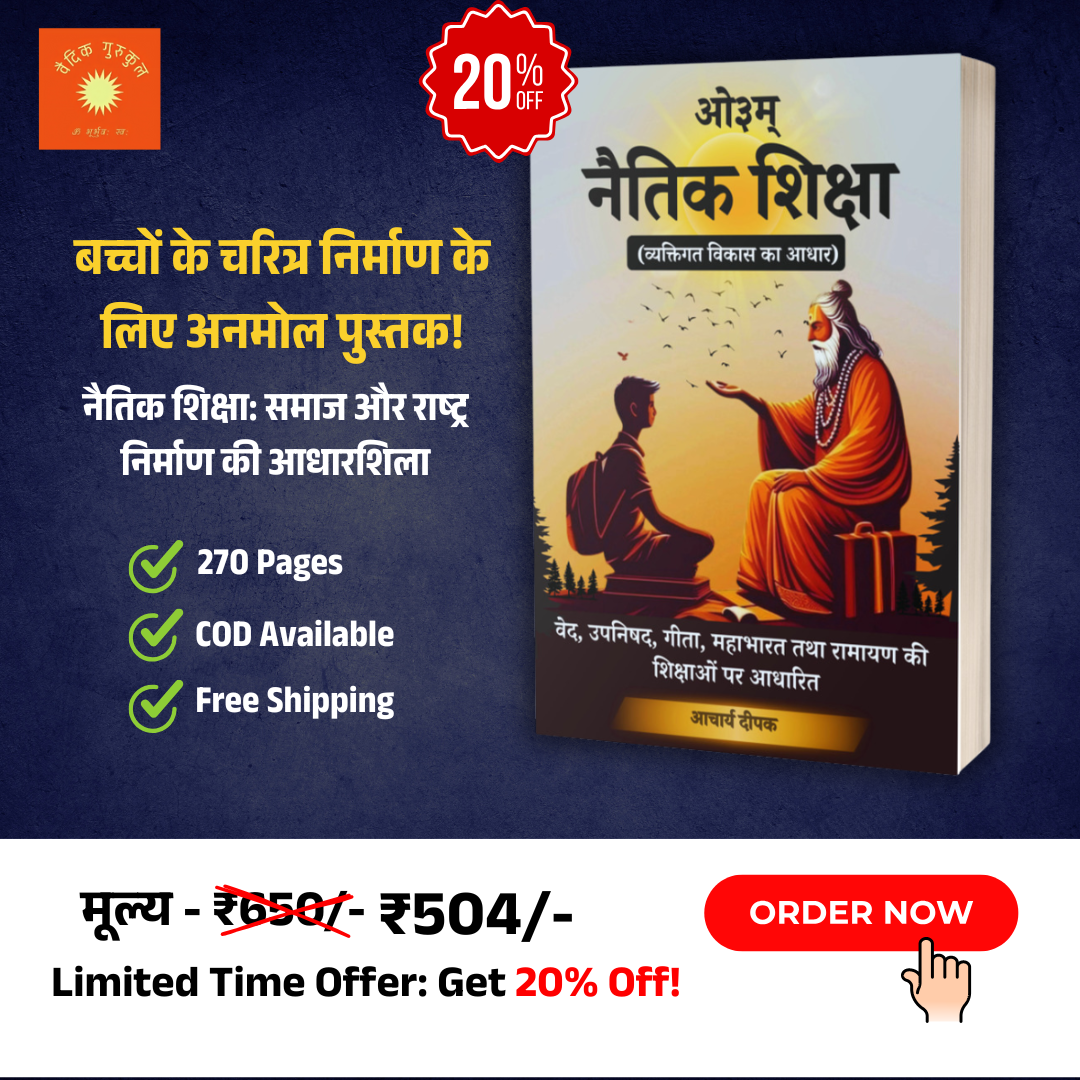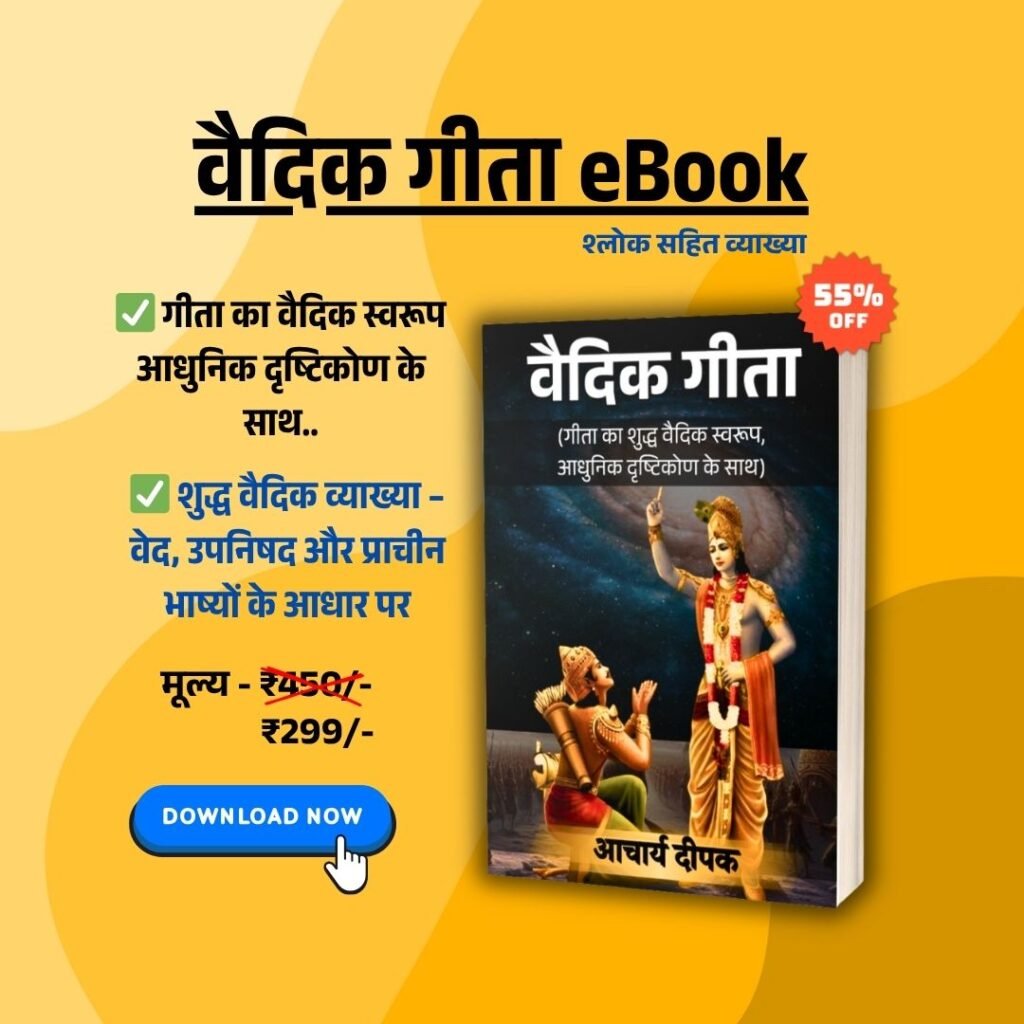Now Reading: अर्जुन और सुभद्रा के विवाह पर उठी शंकाओं का तर्कसंगत समाधान
-
01
अर्जुन और सुभद्रा के विवाह पर उठी शंकाओं का तर्कसंगत समाधान
अर्जुन और सुभद्रा के विवाह पर उठी शंकाओं का तर्कसंगत समाधान

भारतीय संस्कृति और विवाह परंपरा की गहराई
भारत (आर्यावर्त) की संस्कृति और परंपरा विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। यह आर्य संस्कृति और वेदों के सिद्धांतों पर आधारित रही है। समय के प्रभाव और वेद विद्या के प्रसार में आई रुकावटों के कारण समाज में अनेक भ्रांतियाँ उत्पन्न हो गईं। इनमें से एक प्रमुख भ्रांति यह है कि अर्जुन ने अपनी ममेरी बहन सुभद्रा से विवाह किया था। इस लेख में हम इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे।
शंका समाधान के चार प्रमुख पहलू
इस विषय की गहन समझ के लिए इसे चार दृष्टिकोणों से देखना आवश्यक है:
- सपिण्ड और गोत्र प्रणाली
- सुभद्रा के माता-पिता को लेकर भ्रम
- कुंती और पृथा के बीच का अंतर
- हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के अनुसार विवाह की वैधता
1. सपिण्ड और गोत्र प्रणाली का विश्लेषण
मनुस्मृति में विवाह संबंधी स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए हैं:
- कन्या माता की ओर से छठी पीढ़ी तक और पिता की ओर से गोत्र संबंधी निषेध के अंतर्गत नहीं होनी चाहिए।
मनुस्मृति का उल्लेख: “असपिण्डा च या मातुरसगोत्र च या पितुः। सा प्रशस्ता द्विजातीनां दारकर्मणि मैथुने।।४।।”
अर्थ: यदि कन्या माता की छह पीढ़ियों तक और पिता के गोत्र में नहीं आती है, तो उसका विवाह उचित है।
गोत्र का विश्लेषण:
- अर्जुन का गोत्र अत्रि था।
- सुभद्रा का गोत्र यदु था।
- चूँकि दोनों अलग-अलग गोत्र से थे, अतः यह विवाह शास्त्रसम्मत था।
2. सुभद्रा के माता-पिता को लेकर भ्रांतियाँ
सुभद्रा के कुल को लेकर शास्त्रों में जितने भी प्रमाण हमें मिलते हैं उनमें अनेक भिन्नताएं हैं
(क) सुभद्रा, वसुदेव और रोहिणी की पुत्री थीं
- यदि सुभद्रा वसुदेव और रोहिणी की पुत्री थीं, तब भी उनका गोत्र अर्जुन से भिन्न था।
- पीढ़ी के अंतर के कारण यह विवाह पूर्णतः मान्य था।
(ख) सुभद्रा, नंद बाबा और यशोदा की पुत्री थीं
- उड़ीसा की महाभारत के अनुसार, सुभद्रा ने स्वयं को नंद बाबा और यशोदा की पुत्री बताया।
- यदि यह सत्य मान लिया जाए, तो अर्जुन और सुभद्रा के बीच कोई रक्त संबंध नहीं था।
3. कुंती और पृथा: एक विश्लेषण
- कुंती का वास्तविक नाम पृथा था और वे शूरसेन की पुत्री थीं।
- कुंती को कुंतिभोज ने गोद लिया, जिससे उनका गोत्र बदल गया।
- दत्तक ग्रहण करने पर नए पिता का गोत्र ही संतान का गोत्र माना जाता है।
- इस कारण अर्जुन और सुभद्रा के विवाह में कोई बाधा नहीं थी।
4. हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के अनुसार वैधता
- पिता की ओर से पाँचवीं पीढ़ी तक और माता की ओर से तीसरी पीढ़ी तक का रक्त संबंध निषिद्ध होता है।
- अर्जुन और सुभद्रा के बीच छह पीढ़ियों का अंतर था, इसलिए विवाह कानूनी रूप से वैध था।
पीढ़ी अंतर का विश्लेषण:
- सुभद्रा की पीढ़ी गणना:
- सुभद्रा
- रोहिणी
- वसुदेव
- शूरसेन
- अर्जुन की पीढ़ी गणना:
- अर्जुन
- कुंती
- शूरसेन
- वसुदेव
- रोहिणी
- सुभद्रा
इसलिए, यह विवाह किसी भी प्रकार से अनैतिक नहीं था और पूर्णतः शास्त्रीय एवं कानूनी दृष्टिकोण से उचित था।
अर्जुन का गोत्र: नियोग परंपरा का प्रभाव
अर्जुन नियोग से उत्पन्न संतान थे, जिनके जैविक पिता तो इंद्र थे, लेकिन समाजिक और गोत्रीय दृष्टि से वे पांडु के पुत्र माने गए।
मत्स्य पुराण के अनुसार: नियोग से उत्पन्न संतान अपने जैविक पिता का नहीं, बल्कि उस कुल के पिता का गोत्र अपनाती है, जहाँ वह जन्म लेती है।
- पांडु का गोत्र अत्रि था।
- अर्जुन ने इसी गोत्र को ग्रहण किया।
- इस कारण अर्जुन और सुभद्रा के बीच विवाह में कोई गोत्रीय बाधा नहीं थी।
निष्कर्ष
- गोत्र और सपिण्ड प्रणाली के अनुसार अर्जुन और सुभद्रा का विवाह वेद सम्मत था।
- सुभद्रा के माता-पिता को लेकर अलग-अलग मत हैं, लेकिन किसी भी स्थिति में वे अर्जुन की सगी बहन नहीं थीं।
- कुंती और पृथा के बीच अंतर के कारण अर्जुन का गोत्र भिन्न हो गया था, जिससे कोई निकट संबंध नहीं बनता।
- भारतीय विवाह अधिनियम के अनुसार भी यह विवाह पूरी तरह वैध था।
इसलिए, यह सोचना कि अर्जुन और सुभद्रा भाई-बहन थे और उनका विवाह अनुचित था, पूर्णतः गलत धारणा है। वेदों और शास्त्रों के अनुसार यह विवाह न केवल उचित था, बल्कि समाज में स्वीकृत भी था।
ऐतिहासिक तथ्यों की प्रामाणिकता और शोध की आवश्यकता
इतिहास में मामा और बुआ के पुत्र-पुत्री के विवाह के अनेकों उदाहरण मिलते हैं, परंतु यह ध्यान रखना आवश्यक है कि वे केवल शरीर के संबंध से रिश्तेदार थे, जबकि गोत्रीय दृष्टिकोण से भिन्न हो सकते थे। इस पर गहन शोध की आवश्यकता है। जब हम जैसे साधारण लोग इस प्रकार के विवाह को सहज स्वीकार नहीं करते, तो योगेश्वर श्रीकृष्ण और वेदों और शास्त्रों के ज्ञाता ऋषि-मुनि इसे कैसे मान्यता देते होंगे? यह विचारणीय प्रश्न है।
आपद्धर्म की रक्षा के लिए विपरीत परिस्थिति में कुछ विवाह हुए भी होंगे, इसकी संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता। इसलिए, विभिन्न कालखंडों के बीच इतना बड़ा अंतर होने के कारण उन परिस्थितियों की सटीक कल्पना और आकलन करना आज के समय में अत्यंत कठिन है। उचित और अनुचित का निर्णय भी वर्तमान संदर्भ में संभव नहीं है, क्योंकि ऐतिहासिक और सामाजिक परिस्थितियाँ समय-समय पर बदलती रही हैं।
इतिहास में समय-समय पर तथ्यों में मिलावट और फेरबदल भी हुई है, जिसके कारण शास्त्रीय प्रमाणों में भी भिन्नताएँ मिलती हैं। वेदों की शिक्षाएँ समय के साथ दुर्लभ हो गईं, जिससे सत्य और मिथ्या के बीच अंतर कर पाना कठिन हो गया। इसलिए किसी भी तथ्य पर आँख मूँदकर विश्वास करने के बजाय उसे तर्क और बुद्धि की कसौटी पर कसना आवश्यक है। सत्य की खोज में तर्क, शास्त्र और प्रमाणों का सम्यक अध्ययन करना चाहिए।
आइए, सत्य की खोज में वेदों की ओर लौटें!