Now Reading: दुख का मूल कारण क्या है? वेदों की दृष्टि से सम्पूर्ण समाधान
-
01
दुख का मूल कारण क्या है? वेदों की दृष्टि से सम्पूर्ण समाधान
दुख का मूल कारण क्या है? वेदों की दृष्टि से सम्पूर्ण समाधान

यदि ईश्वर करुणामय है तो सृष्टि में इतना दुःख क्यों है? यह प्रश्न केवल आधुनिक चिंतन नहीं, अपितु ऋषियों, मुनियों, तत्त्वचिंतकों, और महान दार्शनिकों के मन में भी उत्पन्न हुआ था। युद्ध, बीमारी, मृत्यु, असमानता, पीड़ा, दरिद्रता, अन्याय — ये सब इस प्रश्न को और तीव्र बनाते हैं।
इस लेख में हम वेद, उपनिषद, भगवद्गीता, दर्शन शास्त्र, और आधुनिक विज्ञान तथा मनोविज्ञान की दृष्टि से इस शाश्वत प्रश्न का समाधान प्रस्तुत करेंगे।
Table of Contents
उपनिषदों में दुख की अवधारणा
वेद दुख को “अविद्या” या “अज्ञान” का परिणाम मानते हैं।
👉 ऋग्वेद में कहा गया है:
“तमसो मा ज्योतिर्गमय”
— बृहदारण्यक उपनिषद् 1.3.28
(अर्थ: मुझे अंधकार (अविद्या, दुख) से ज्ञान (प्रकाश) की ओर ले चलो)
स्पष्टीकरण:
वेद कहते हैं कि सृष्टि का उद्देश्य ‘अनुभव’ है — और यह अनुभव तभी संभव है जब व्यक्ति सुख और दुख दोनों को जान सके। यदि केवल सुख ही हो, तो उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। इसलिए, दुख आत्मा के अनुभव-विकास की प्रक्रिया का एक अंग है।
उपनिषदों की दृष्टि: आत्मा और माया
👉 मुण्डक उपनिषद कहता है:
“द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया…”
(दो पक्षी — आत्मा और जीव — एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। एक फल खाता है (दुख-सुख अनुभव करता है), दूसरा केवल देखता है।)
इस श्लोक के माध्यम से यह बताया गया है कि जीवात्मा माया के कारण फल (दुख-सुख) का भोक्ता बनती है, जबकि परमात्मा साक्षी रूप में स्थित रहता है।
मुख्य कारण:
- आत्मा शुद्ध है, परंतु जब वह माया से आच्छादित होती है, तब वह अपने को ‘देह’ समझती है।
- इसी देहाभिमान से काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार उत्पन्न होते हैं — जो दुख के कारण बनते हैं।
भगवद गीता में दुख की व्याख्या
भगवद गीता दुख को मानसिक भ्रम और ममता का परिणाम मानती है।
👉 श्रीकृष्ण अर्जुन से कहते हैं:
“हे अर्जुन! सुख-दुख, सर्दी-गर्मी, लाभ-हानि तो अस्थायी हैं, इन्हें सहन करो।” — गीता 2.14
“अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे।” — गीता 2.11
(तू जिनके लिए शोक कर रहा है, वे शोक करने योग्य नहीं हैं)
गीता के अनुसार दुख के कारण:
- मोह (Attachment): जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से अत्यधिक जुड़ जाते हैं।
- अहम (Ego): जब हम अपने को कर्ता मानते हैं।
- फल की इच्छा: कर्म तो ठीक है, लेकिन फल की आसक्ति दुख का कारण बनती है।
योग दर्शन: क्लेश और दुख
महर्षि पतंजलि के योगसूत्र में दुख के पाँच मूल कारण (क्लेश) बताए गए हैं:
“अविद्या-अस्मिता-राग-द्वेष-अभिनिवेशाः पंचक्लेशाः”
— योगसूत्र 2.3
इनका अर्थ:
- अविद्या: सत्य को न जानना
- अस्मिता: ‘मैं’ का भाव
- राग: सुख देने वाली वस्तु की तृष्णा
- द्वेष: दुख देने वाली वस्तु से द्वेष
- अभिनिवेश: मृत्यु का भय
👉 जब तक ये पंच क्लेश जीव में विद्यमान हैं, तब तक दुख बना रहेगा। योग के अभ्यास द्वारा ही इनका क्षय होता है।
आधुनिक विज्ञान की दृष्टि
न्यूरोसाइंस:
- मस्तिष्क में Amygdala दुख व भय के अनुभवों को संचित करता है।
- नकारात्मक अनुभव मस्तिष्क में तेज़ी से छपते हैं (Negative Bias) ताकि जीव रक्षा कर सके।
मनोविज्ञान:
- दुख एक चेतावनी है कि जीवन की दिशा बदलनी चाहिए।
- आधुनिक मनोवैज्ञानिकों जैसे विक्टर फ्रैंकल का मानना है कि “दुख को अर्थ देने से वह सहनीय हो जाता है।”
“He who has a why to live can bear almost any how.” – Nietzsche
वेदों में दुख शमन का उपाय: मंत्रों की शक्ति
वेद केवल दुख के कारणों का विश्लेषण ही नहीं करते, बल्कि उनके समाधान भी प्रस्तुत करते हैं। ऋग्वेद में एक अत्यंत प्रभावशाली मंत्र आता है जो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दुखों को शांत करने की प्रार्थना के रूप में प्रयुक्त होता है:
ऋग्वेद 10.137.3
“अभि त्वा सूक्तैः शमयामि वातापेमसि शमितः स्याम।
शं नो भव द्विपदे शं चतुष्पदे॥”
भावार्थ:
“हे रोग व दुख! मैं तुझे वेद मंत्रों के प्रभाव से शांत करता हूँ।
तू शांत हो, हम भी शांति को प्राप्त हों।
हमारे लिए और समस्त प्राणियों के लिए — दोपद (मनुष्य) और चतुष्पद (पशु) — शुभता और शांति हो।”
यह मंत्र क्या दर्शाता है?
- दुख केवल एक व्यक्तिगत अनुभूति नहीं, बल्कि समाज और प्रकृति से जुड़ा हुआ अनुभव है।
- इस मंत्र में ध्वनि (मंत्र शक्ति) को एक उपचारात्मक शक्ति माना गया है।
- यह हमें सिखाता है कि दुख का समाधान केवल तर्क या क्रिया से नहीं, बल्कि सद्भाव, शांति और चेतना से भी संभव है।
इसका व्यवहारिक पक्ष:
आज के युग में जब मानसिक तनाव, चिंता और सामाजिक विघटन बढ़ रहा है, तो इस प्रकार के वैदिक मंत्र मनोवैज्ञानिक उपचार, ध्यान और प्रार्थना चिकित्सा में अत्यंत सहायक हो सकते हैं। कई योग एवं आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धतियाँ इन्हें मंत्र चिकित्सा (Mantra Healing) के रूप में प्रयोग करती हैं
कर्म सिद्धांत और पुनर्जन्म
सनातन धर्म के अनुसार, हर दुख का कारण कोई पूर्वकर्म है।
👉 मनुस्मृति में कहा गया है:
“सर्वे कर्माणि जन्तूनां शुभाशुभफलोद्भवाः।”
(सभी प्राणी अपने कर्मों के अनुसार सुख-दुख पाते हैं)
- यदि किसी जन्म में हिंसा की है, तो अगले जन्म में उसका फल भोगना ही पड़ेगा।
- कर्म नष्ट नहीं होते, वे संस्कार के रूप में चित्त में रहते हैं और अवसर पाकर फल देते हैं।
संसार की स्वभाविक प्रकृति: परिवर्तनशीलता
दुख का मुख्य कारण यह है कि हम अनित्य वस्तुओं से नित्य सुख की अपेक्षा करते हैं।
“संसार दुःखमय है, क्योंकि सब कुछ नश्वर है।”
वेदों में भी यही बात ‘अनित्यता’ के रूप में बताई गई है।
“यद्नश्वरं तददुखरूपं” — (जो नश्वर है, वह दुखदायक है)
इसलिए दुख से बचना है, तो स्थायी तत्व — आत्मा या ब्रह्म — की ओर जाना चाहिए।
क्या भगवान दोषी हैं?
यह प्रश्न प्रायः पूछा जाता है – “क्या भगवान ने दुखों से भरी सृष्टि बनाई है?”
👉 उत्तर: नहीं।
ईश्वर ने नियमों से युक्त एक न्यायपूर्ण सृष्टि बनाई है।
हर आत्मा स्वतंत्र है — वह जैसा कर्म करेगी, वैसा फल पाएगी।
“नादत्ते कस्यचित्पापं न चैव सुकृतं विभुः।” — गीता 5.15
(ईश्वर किसी के पाप या पुण्य को नहीं लेता। हर आत्मा स्वयं उत्तरदायी है)
वैदिक समाधान: दुख से मुक्ति कैसे?
1. ज्ञान का मार्ग (Jnana Yoga):
- आत्मा और शरीर को अलग समझना
- ‘मैं’ शरीर नहीं, आत्मा हूँ — यह समझते ही दुख क्षीण हो जाता है
2. कर्म योग:
- निष्काम भाव से कार्य करना
- फल की चिंता न करके कर्तव्य पर ध्यान देना
3. भक्ति योग:
- ईश्वर में पूर्ण समर्पण से मानसिक शांति
- दुख ईश्वर की परीक्षा समझकर सहज भाव रखना
4. योग साधना:
- ध्यान, प्राणायाम और यम-नियम से क्लेशों का क्षय
- स्थिर और समभावी मन प्राप्त करना
निष्कर्ष
दुख एक दंड नहीं, अपितु आत्मा की यात्रा में एक अवसर है —
👉 सीखने का, बढ़ने का, और अपने शुद्ध स्वरूप को पहचानने का।
🌼 वेद, उपनिषद, गीता, योग-दर्शन, सभी एक स्वर में कहते हैं:
“दुख असत्य नहीं है, परंतु उसका समाधान संभव है।”
“दुख से मुक्त होना, मानव जीवन का परम लक्ष्य है।”
📚 संदर्भ ग्रंथ
- भगवद गीता – श्रीकृष्ण उपदेश
- उपनिषद – बृहदारण्यक, मुण्डक
- पतंजलि योगसूत्र
- मनुस्मृति
- ऋग्वेद व यजुर्वेद
- विक्टर फ्रैंकल: Man’s Search for Meaning
- भगवद्पाद शंकराचार्य की अद्वैत व्याख्या
समापन
यदि हम वेदों की गहराई से इस विषय को समझें, तो हमें यह ज्ञात होता है कि सृष्टि में दुख स्थायी नहीं, साधन है — आत्मा को परमात्मा तक पहुँचाने का।
इसलिए, दुख को शत्रु नहीं, गुरु मानिए। वह हमें अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य की ओर प्रेरित करता है।




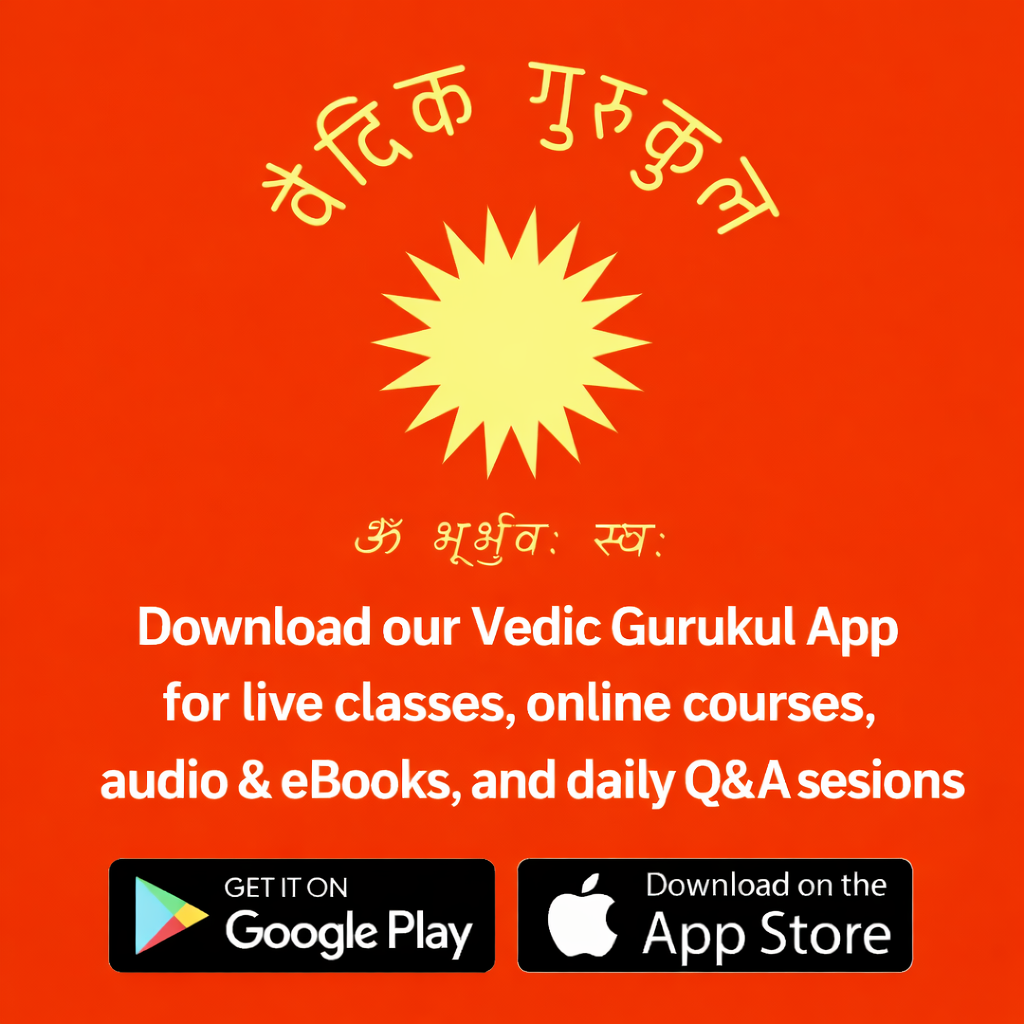

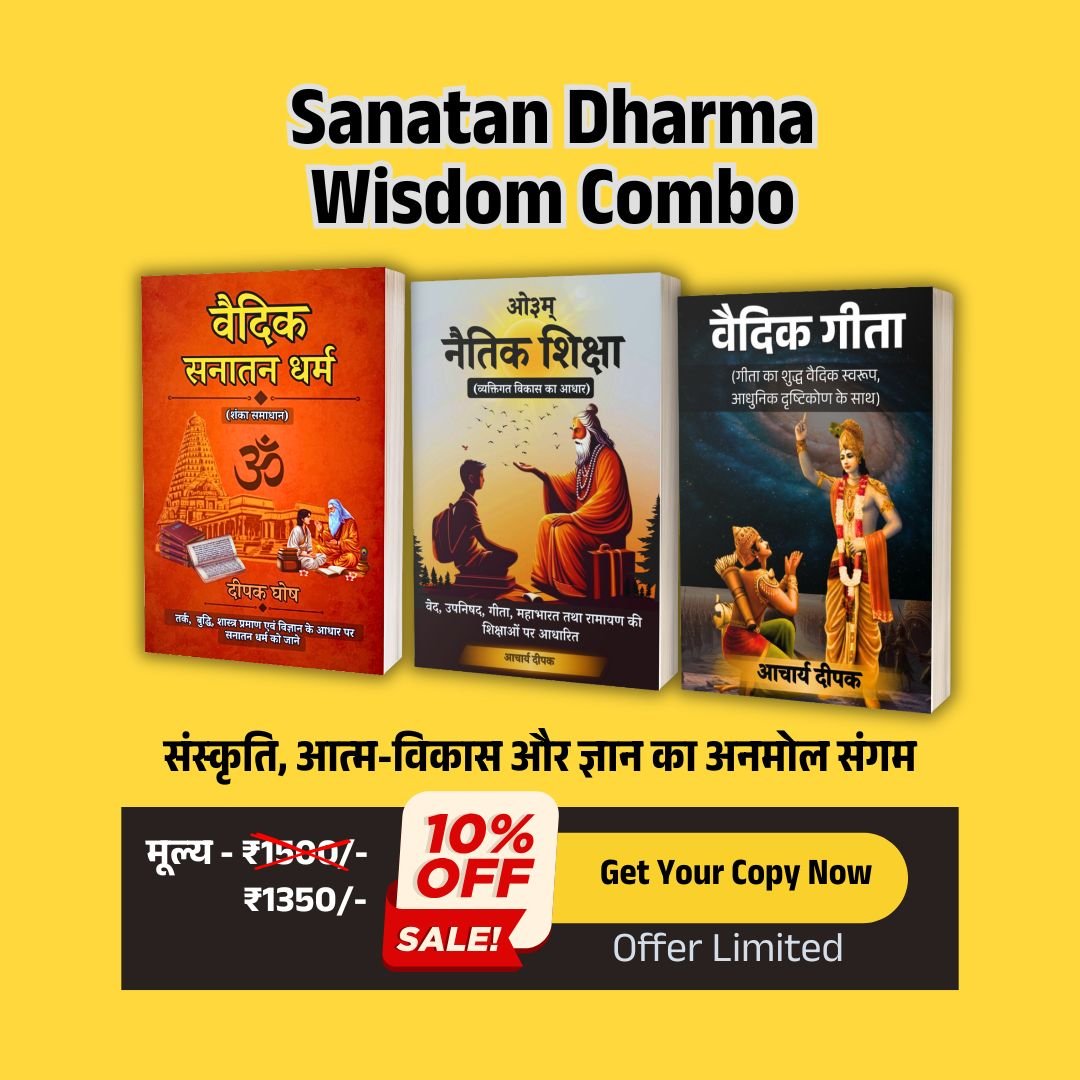
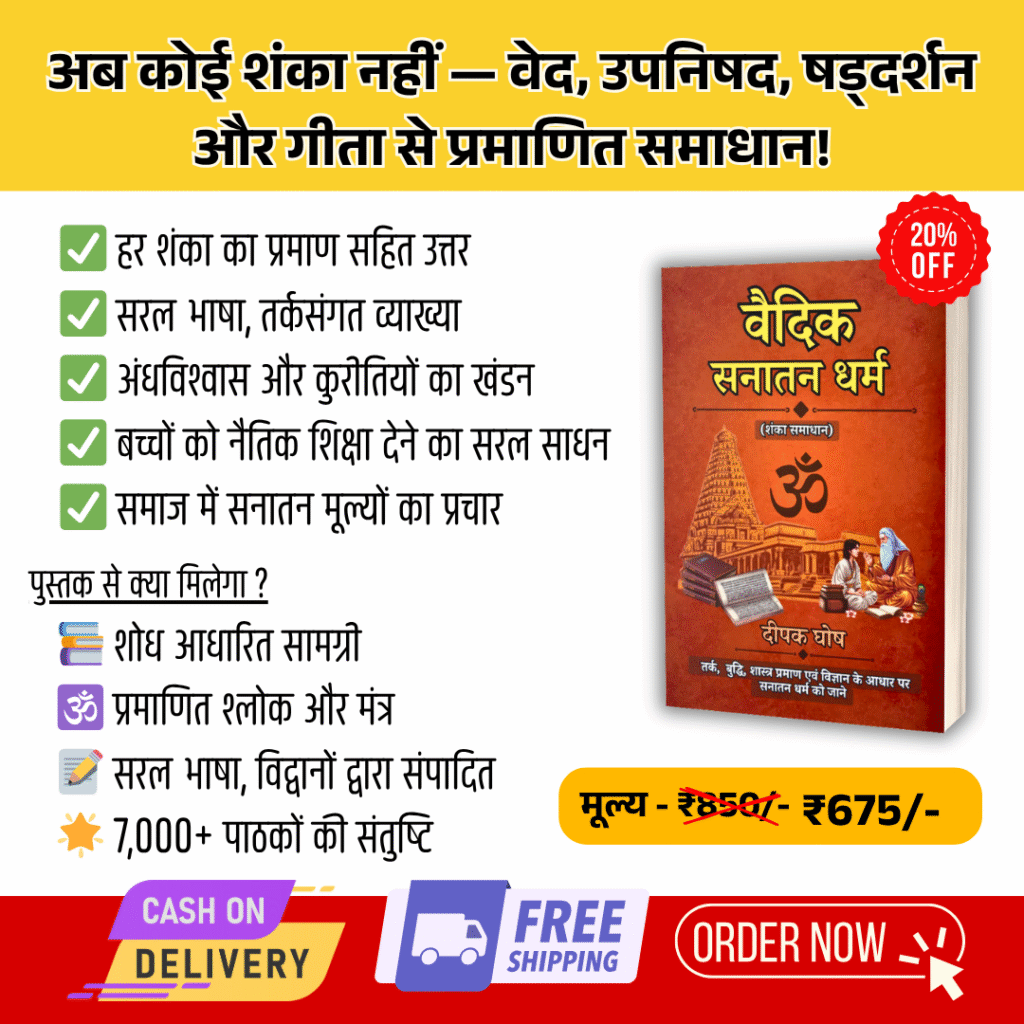
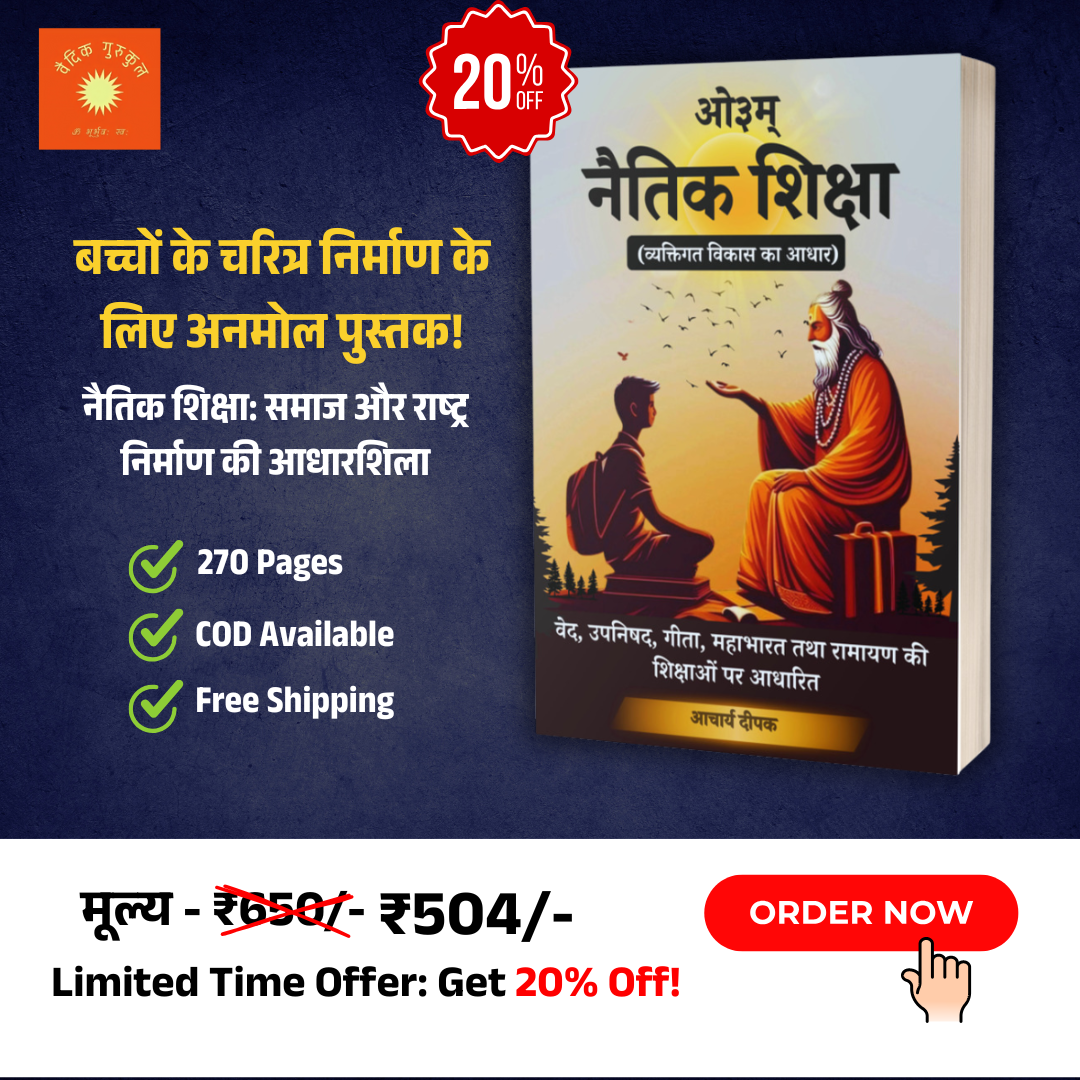
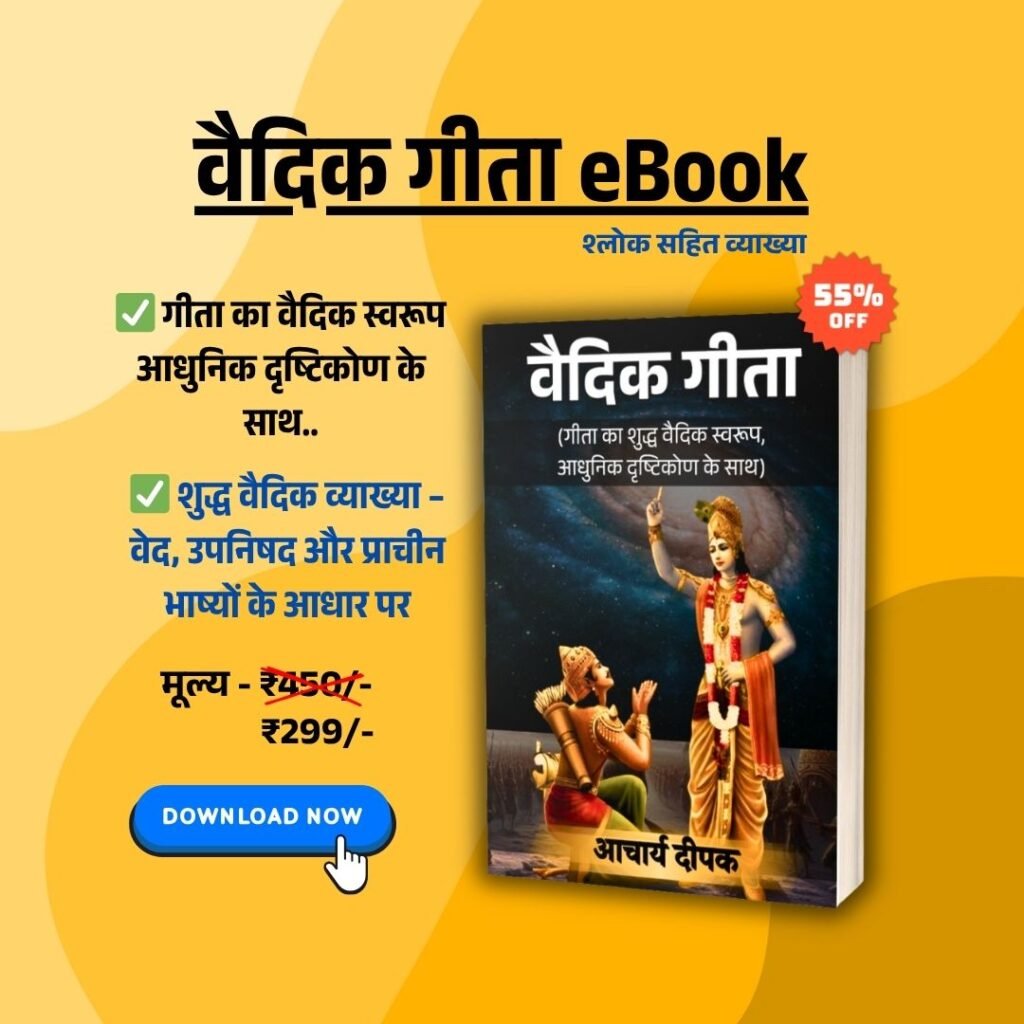














Sagar Sinha
Very nice post गुरुजी 🙏